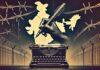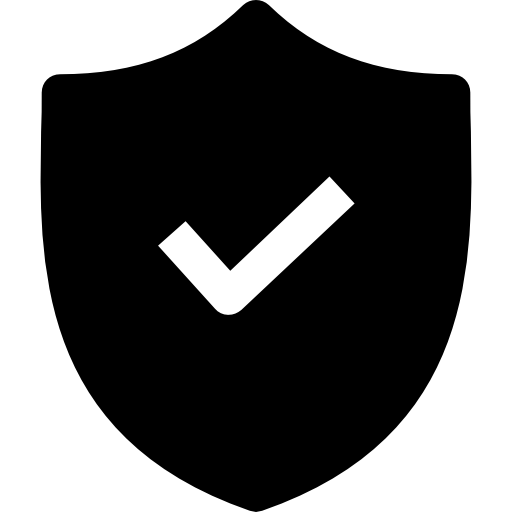नई डिजिटल तकनीकी क्रांति के प्रभाव से वैश्विक पूंजीवाद के भीतर हो रहे परिवर्तनों को समझने के लिए विशेषज्ञ लगे हुए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ‘एल्गोरिद्म पूंजीवाद’, ‘संज्ञानात्मक पूंजीवाद’, ‘संचार पूंजीवाद’, ‘डेटा पूंजीवाद’, ‘डिजिटल पूंजीवाद’, ‘प्रतिरोधहीन पूंजीवाद’, ‘सूचनात्मक पूंजीवाद’, ‘प्लेटफ़ॉर्म पूंजीवाद’, ‘अर्द्ध-पूंजीवाद’, ‘नियंत्रक पूंजीवाद’ और ‘आभासी पूंजीवाद’ जैसे कुछ नाम और विशेषण अनेक विशेषज्ञों ने और कुछ मसखरों ने दे भी डाले हैं। हाल ही में पूंजीवाद के वर्गीकरण की जो नई अवधारणा प्रस्तुत की गई है वह उसके प्रचलित अर्थों को पीछे छोड़ देती है।
यह नयी अवधारणा पूंजीवाद से आगे की भावना वाली नहीं है। फिलहाल तो इसे डेटा की पूंजी बनाने वालों और अंतर्जाल – नेट – पर जानकारियां हासिल करने वाले उपयोगकर्ताओं की दुनिया के लिए एक प्रतिगामी कदम के रूप में ही देखा जा रहा है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वाम और दक्षिण दोनों पंथों के लिए ‘डिजिटल सामंतवाद’, ‘तकनीकी-सामंतवाद’, ‘सूचना सामंतवाद’, ‘नव-सामंतवाद’ नये संकेत शब्द बन गए हैं। अकादमिक तथा बुद्धिजीवी लोग मानते हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के सबसे उन्नत क्षेत्रों की अवधारणा को अभी ठीक-ठीक समझना बाकी है। इसमें वामपंथियों के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग वाले दिग्गज भी अभी अंधेरे में ही भटक रहे हैं कि इसे कैसे समझा जाय और कैसे लिया जाय! उनके सामने मुश्किल यह है कि गूगल, अमेजॉन, और फ़ेसबुक जैसे विराट सूचना-तकनीकी प्लेटफॉर्म जो पुराने जमाने के श्रमिकों के पूंजीवादी शोषण की तरह अपना मुनाफा नहीं बनाते हैं, तो क्या उन्हें जमींदारी के नए मॉडल के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसे गैर-उत्पादक मालिक के रूप में, जो अपने नेटवर्क-प्रभुत्व और एकाधिकार की पकड़ का लाभ उठाते हुए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी और जगह से उत्पन्न विज्ञापन से आय पाने के लिए ‘डेटा-सेट’ और ‘एल्गोरिद्म’ पर निर्भर करते है? या वे एल्गोरिद्म निगरानी के जरिये उपयोगकर्ता के डेटा को संकलित करने और उन्हें उड़ा ले जाने से अमीर बन रहे हैं? बेदखल करके संग्रह करने की पुरानी प्रवत्ति की ही भांति क्या यह डिजिटल बेदखली नहीं है?
यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि इक्कीसवीं सदी के तकनीकी दिग्गजों ने सूचना और ज्ञान पर अपने नियंत्रण अर्थात ‘बौद्धिक एकाधिकार’ से हमें प्रभावी ढंग से अपने अधीन कर लिया है और अब वे उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हुए बिना भी बड़ी खूबसूरती से ‘सरप्लस मूल्य’ हासिल कर लेते है। इसे समझने के लिए गूगल का उदाहरण लिया जा सकता है। डेटा एकत्र करने पर गूगल के एकाधिकार का व्यवसाय मॉडल काफी हद तक किसी वस्तु के उत्पादन पर निर्भर करता है और वह है ‘खोज परिणाम’ यानी ‘सर्च रिज़ल्ट’ या यूं कहें कि ‘मानव ज्ञान के विशाल भंडार तक वास्तविक समय में पहुंच’। गूगल इसे ‘मुफ़्त’ उपलब्ध कराता है ताकि वह विज्ञापनदाताओं को अपने उपयोगकर्ताओं तक लक्षित पहुंच देने की बिक्री कर सके। किन्तु इसे क्लासिकल बौद्धिक एकाधिकार नहीं कह सकते क्योंकि जिन वेब पेजों को गूगल क्रमबद्ध करता है वे उनके बनाने वालों की अमूर्त संपत्ति बनी रहती है। उन्हें वास्तव में तो अपनी संपत्ति के उपयोग करने वाले गूगल से किसी भी लाइसेंस शुल्क पाने का अधिकार छोड़ना पड़ता है। इसी पृष्टभूमि में अब वैचारिक जगत में इस बात पर बहस शुरू हुई है कि हमारा आधुनिक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से एक सामंती शक्ति के रूप में संगठित हो रहा है और वह हमारी मौजूदा शक्ति संरचनाओं और स्वतंत्रता को चुनौती देने लगा है।
सामंतवाद की सामान्य अवधारणा यह है कि स्वामित्व वाला एक अपेक्षाकृत छोटा वर्ग उत्पादक वर्ग से काम लेकर बिना कुछ किए धरे मुनाफा कमाता है। इसके लिए यह वर्ग विभिन्न प्रकार की परोक्ष और अपरोक्ष रूप से राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का उपयोग करता है। दूसरी तरफ उत्पादक वर्ग के पास आम तौर पर बहुत कम विकल्प होते हैं और वह प्रभावशील नहीं होता है। डिजिटल जगत में उपयोगकर्ता ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं तब उन्हें अक्सर पता ही नहीं होता कि ऐसा करते हुए वे अपने कितने डेटा प्लेटफ़ॉर्म चलाने वालों के साथ साझा कर दे रहे होते हैं। इन डेटा का उपयोग प्लेटफ़ॉर्म के मालिक अपने लिए मूल्य पैदा करने के लिए करते हैं। हमारे वर्तमान डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और सामंती समाजों के बीच इतनी अधिक समानताएं हैं कि यह बेहिचक कहा जा सकता है कि डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, विशेष रूप से सोशल मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र, एक वास्तविक सामंती समाज विकसित कर रहा है। आधुनिक सोशल मीडिया और उसके डेटा विज्ञान का पारिस्थितिकी तंत्र सामंती सामाज और आर्थिक व्यवस्था के ढांचे की ही झलक देता हैं। पुराने सामंती ज़माने में किसान-मजदूर लोग खेती, पशुपालन और कारखानों में अपने श्रम का समर्पण करते थे। अब इस नई प्रणाली में डेटा उत्पादन और समर्पण का काम होता है। इस प्रणाली के स्वामी टेक कंपनियों के संचालक होते हैं। इसीलिए यह भी माना जा रहा है कि यह संपूर्ण बुनियादी ढांचा उपयोगकर्ता के डेटा का संग्रह करने और उसके शोषण पर खड़ा है।
बाज़ार की ताकतें दावा करती हैं कि सोशल मीडिया में तो “स्वैच्छिक भागीदारी” या सहमति होती है। यहां कोई किसी को मजबूर नहीं करता जैसे पुराने जमाने में जमींदार करते थे। डेटा साइंस और सोशल मीडिया इकोसिस्टम पर चर्चा करने वाले किसी भी व्यक्ति के सामने अनिवार्य रूप से यही तर्क रखा जाता है कि सोशल मीडिया में तो भागीदारी स्वैच्छिक है। फौरी तौर पर देखने पर यह एक प्रभावी तर्क लगता है। लेकिन यह भी सभी जानते हैं कि सामान्यतः सहमति टूटती है और आधुनिक डिजिटल डेटा व्यवस्था में आम भागीदार की निजता कोई महत्व नहीं रखती। इसलिए नई प्रौद्योगिकी जनित डिजिटल मीडिया में राजनीति, नैतिकता और मूल्यों के अंतरसंबंधों की भी बड़ी समस्या है। डेटा की साझेदारी की सहमति को मध्ययुगीन किसानों के “स्वेच्छा से” अपना श्रम देने के समान ही देखा जा सकता है। वहां स्वेच्छा नहीं थी, मजबूरी थी। आज भी खुद का डेटा देने के लिए एक तरह से बाध्यता ही है। उपयोगकर्ता की जानकारी पाने के लिये उसे अपना डेटा सौंपने के लिए क्लिक करवा ही लिया जाता है। हालांकि मध्ययुगीन समाज की तुलना में आधुनिक समाज में हालत वैसी क्रूर नहीं है जैसे जागीरदारों के आतंकी काल में होती थी। अब लगभग सभी व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार डिजिटल होने लगे हैं, उनमें शामिल न होने की छूट होती है किन्तु ऐसा करने से इनकार करने वाला उस व्यवस्था से बाहर हो जाता हैं। समकालीन समाज में यह लगभग असंभव है कि कोई डिजिटल व्यवस्था में भागीदारी न करने का विकल्प चुने। क्योंकि सरकारें भी आम नागरिक से संपर्क डिजिटल मंच पर करने लगी हैं। संदेश भेजने और सूचनाएं पाने के डिजिटल मंच तो अब जीवन की जरूरत बन गये हैं। अब तो सरकारी नौकरियों के लिए तथा शिक्षण संस्थानों में आवेदन भी ऑनलाइन ही करने पड़ते हैं। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई विकलांग और अन्य व्यक्तियों के लिए, डिजिटल जरिया ही एकमात्र विकल्प है, जो उन्हें मजबूरन पूर्ण समर्पण की ओर ही धकेलता है। आधुनिक इंटरनेट के साथ यह चेतावनी हमेशा होती है कि जो कुछ भी ऑर्डर किया जाता हैं या कहा जाता हैं, उसे कोई ट्रैक करेगा, चाहे वह किसी के जीवन के लिए कितना भी आवश्यक क्यों न हो। नेट के उपयोगकर्ता के पास यह विकल्प ही नहीं बच रहा है कि वह उसमें शामिल न हों। भागीदारी के संदर्भ में, मध्ययुगीन सामंतवाद और डिजिटल सामंतवाद के बीच सिर्फ यही अंतर है कि कोई भी व्यक्ति अब केवल एक मंच के साथ बंधा नहीं है। इसके बजाय, प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न डिजिटल प्रबंधकों के लिए उसके दायित्वों का एक जाल होता है, जिनमें से प्रत्येक उपयोग के बदले में अलग-अलग डेटा की मांग होती है जिसे पूरी करनी पड़ती है। जिन लोगों के गोपनीयता से सरोकार हैं, उनके लिए सवाल यह है कि वे अपने कितने डेटा को सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और क्या उनका व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन उनके निर्णयों के अनुकूल है।
परंपरागत रूप से, जब कर्मचारी काम कर रहे होते हैं तब उनका समय उनका अपना नहीं होता है, और उसके नियोक्ता को उसके सामान्य कार्यक्रम, उसकी उत्पादन क्षमता और कार्य शैली के बारे में सब पता होता है। लेकिन अब नियोक्ता के अलावा एक अन्य तीसरे-पक्ष या कंपनी को भी उन सभी चीज़ों की जानकारी होती है, और वे आपके डेटा को अन्य कंपनियों से एकत्रित किए गये डेटा के साथ साझा कर सकते हैं। किसी कर्मचारी का समय और कार्य आउटपुट उसके नियोक्ता से संबंधित तो हो सकता है, लेकिन अब कोई और कंपनी भी उनका उपयोग करती है। व्यावसायिक वातावरण में क्लाउड-आधारित सेवाओं से यह नई स्थिति बन गई है। पहले के संप्रभु डिजिटल वातावरण में स्थानीय कॉर्पोरेट सर्वर के पास डेटा भंडारण के दायित्व और अधिकार होते थे मगर अब इन दायित्वों तथा अधिकारों का उपयोग तीसरा पक्ष करता है। यह भी सच है कि कई मामलों में, आपका नियोक्ता ठीक उसी स्थिति में हो सकता है जैसे आप अपने डेटा को सौंपने के मामले में हैं। अब तो ‘ऑफिस 365’ जैसी क्लाउड-आधारित सेवाएं व्यवसायों को आक्रामक रूप से अपनी तरफ खींच रही हैं जिसमें उपयोगकर्ता का निर्णय कोई मायने नहीं रखता। डेटा संग्रहण कंपनियां जोर देती हैं कि किसी एक व्यक्ति के डेटा का कोई सार्थक मूल्य नहीं है। उनका मूल्य कुल मिलाकर बनाता है। इस ‘ब्लाइंड स्पॉट’ का फायदा उठाया जाता है। व्यक्तिगत डेटा कार्यात्मक रूप से किसी काम का नहीं हो लेकिन कुल डेटा बड़ी कंपनियों के मूल्यांकन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है। यही डिजिटल सामंतवाद है।