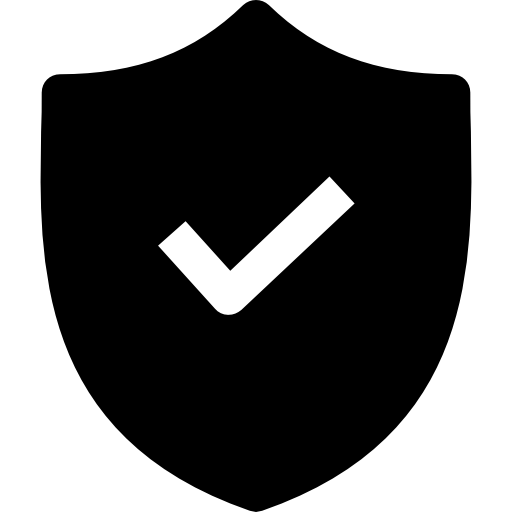इस साल मौसम को ले कर सारे पूर्वानुमान गड़बड़ा रहे हैं। जब भारी गर्मी का अंदेशा था तो वैशाख के महीने में सावन जैसी झड़ी लग गई है. शक लग रहा है कि कहीं अब गर्मी और बरसात का गणित कुछ गडबडा ना जाये, समझ लें कोई साल बारिश का रूठ जाना तो कभी ज्यादा ही बरस जाना जलवायु परिवर्तन के दिनों-दिन बढ़ रहे खतरे का स्वाभाविक परिणाम है और भारत अब इसकी भीषण चपेट में है। इस बार अप्रेल के के पहले हफ्त में ही सदानीरा कहलाने वाली गंगा घाटों से दूर हो गई है। प्रयागराज हो या फिर पटना हर जगह गंगा में टापू नजर आ रहे हैं। अधिकांश छोटी नदियां सूख गई है। और इसका सीधा असर तालाब-कुओं-बावड़ियों पर दिख रहा है। स्काई मेट के अनुसार इस साल देश में सामान्य अर्थात कोई 96 फीसदी बरसात का अनुमान है।
लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सीजन की दूसरी छमाही के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इस बीच, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने भारत के उपजाऊ उत्तरी, मध्य और पश्चिमी मैदानी इलाकों में गेहूं जैसी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे हजारों किसानों को नुकसान हुआ है। भारत के लगभग आधे से ज्यादा किसान अपन खेत में चावल, मक्का, गन्ना, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों को उगाने के लिए वार्षिक जून-सितंबर बारिश पर निर्भर करते है। स्काईमेट को उम्मीद है कि देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में बारिश की कमी का खतरा बना रहेगा।

अप्रेल महीने के अंत में केंद्र सरकार का रिकार्ड बताता है कि संरक्षित जलाशयों का जल स्तर बहुत कम है। उत्तर क्षेत्र , जिसमें हिमाचल. प्न्ज्बा आदि राज्य आते हैं, में 10 जलाशयों की कुल क्षमता का महज 38 प्रतिशत पानी ही बचा है। पूर्वी भारत के 21 जलाशयों में 34 प्रतिशत , पश्चिमी क्षेत्र के 49 जलाशयों में 38 प्रतिशत , मध्य भारत के 26 जलाशयों में 43 और दक्षिण के 40 जलाशयों मने महज 36 प्रतिशत जल शेष है। अभी हिंदी पट्टी में बरसात होने में कम से कम 100 दिन हैं और जान लें कि अगले पंद्रह दिनों में ही जल संकट हर दिन गहरा होता चला जाएगा।
हमारे देश की नियति है कि थोड़ा ज्यादा बादल बरस जाएँ तो उसके समेटने के साधन नहीं बचते और कम बरस जाए तो ऐसा रिजर्व स्टॉक नहीं दिखता जिससे काम चलाया जा सके। अनुभवों से यह तो स्पष्ट है कि भारीभरकम बजट, राहत, नलकूप जैसे शब्द जल संकट का निदान नहीं है। करोड़ों-अरबों की लागत से बने बाँध सौ साल भी नहीं चलते, जबकि हमारे पारंपरिक ज्ञान से बनी जल संरचनांए ढेर सारी उपेक्षा, बेपतवाही के बावजूद आज भी पानीदार हैं। यदि भारत का ग्रामीण जीवन और खेती बचाना है तो बारिष की हर बूंद को सहेजने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यही हमारे पुरखों की रीत भी थी।
बुंदेलखंड में करोड़ों के राहत पैकेज के बाद भी पानी की किल्लत के चलते निराशा, पलायन व बेबसी का आलम है। देश के बहुत बड़े हिस्से के लिए अल्प वर्षा नई बात नही है और ना ही वहां के समाज के लिए कम पानी में गुजारा करना, लेकिन बीते पांच दशक के दौरान आधुनिकता की आंधी में दफन हो गए हजारों चंदेल-बुंदेला कालीन तालाबों और पारंपरिक जल प्रणालियों के चलते यह हालात बने।
मप्र के तीन लाख की आबादी वाले बुरहानपुर शहर में कोई अठारह लाख लीटर पानी प्रतिदिन एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से वितरित होता है जिसका निर्माण सन 1615 में किया गया था। यह प्रणाली जल संरक्षण और वितरण की दुनिया की अजूबी मिसाल है, जिसे ‘भंडारा’ कहा जाता है। जिस जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट के सामने आधुनिक तकनीक बेबस दिखती है, हमारे पुरखे हजारों साल पहले इससे वाकिफ थे और उन्होंने देश -काल-परिस्थिति के अनुसार बारिश को समेट कर रखने की कई प्रणालियां विकसित व संरक्षित की थीं। घरों की जरूरत यानि पेयजल व खाना बनाने के लिए मीठे पानी का साधन कुआं कभी घर-आंगन में हुआ करता था। धनवान लोग सार्वजनिक कुएं बनवाते थे। हरियाणा से मालवा तक जोहड़ या खाल जमीन की नमी बरकरार रखने की प्राकृतिक संरचना हैं। ये आमतौर पर वर्षा -जल के बहाव क्षेत्र में पानी रोकने के प्राकृतिक या कृत्रिम बांध के साथ छोटा तालाब की मानिंद होता है। तेज ढलान पर तेज गति से पानी के बह जाने वाले भूस्थल में पानी की धारा को काटकर रोकने की पद्धति ‘‘पाट’’ पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय रही है। एक नहर या नाली के जरिये किसी पक्के बांध तक पानी ले जाने की प्रणाली ‘‘नाड़ा या बंधा’’ अब देखने को नहीं मिल रही है। कुंड और बावड़िया महज जल संरक्षण के साधन नहीं,बल्कि हमारी स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना रहे हैं।इनडोर में एक ऐसी ही जल युक्त बावड़ी पर अवैध निर्माण कर बने मंदिर के धंसने से 50 से अधिक लोग क्या मरे, शाशन ने उस बावड़ी मो ही मिटटी से भर दिया। जबकि आज जरूरत है कि ऐसी ही पारंपरिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के लिए खास योजना बनाई जाए व इसकी जिम्मेदारी स्थानीय समाज की ही हो।
यह देश -दुनिया जब से है तब से पानी एक अनिवार्य जरूरत रही है और कम बरसात, मरूस्थल, जैसी विषमताएं प्रकृति में विद्यमान रही हैं- यह तो बीते दो सौ साल में ही हुआ कि लोग भूख या पानी के कारण अपने पुश्तैनी घरों- पिंडों से पलायन कर गए। उसके पहले का समाज तो हर तरह की जल-विपदा का हल रखता था। अभी हमारे देखते-देखते ही घरों के आंगन, गांव के पनघट व कस्बों के सार्वजनिक स्थानों से कुएं गायब हुए हैं। बावड़ियों को हजम करने का काम भी आजादी के बाद ही हुआ। हमारा आदि-समाज गर्मी के चार महीनों के लिए पानी जमा करना व उसे किफायत से खर्च करने को अपनी संस्कृति मानता था। वह अपने इलाके के मौसम, जलवायु चक्र, भूगर्भ, धरती-संरचना, पानी की मांग व आपूर्ति का गणित भी जानता थ। उसे पता था कि कब खेत को पानी चाहिए और कितना मवेषी को और कितने में कंठ तर हो जाएगा। आज भी देष के कस्बे-षहर में बनने वाली जन योजनाओं में पानी की खपत व आवक का वह गणित कोई नहीं आंक पाता है जो हमारा पुराना समाज जानता था।

राजस्थान में तालाब, बावड़ियां, कुई और झालार सदियों से सूखे का सामना करते रहे। ऐसे ही कर्नाटक में कैरे, तमिलनाडु में ऐरी, नगालेंड में जोबो तो लेह-लद्दाक में जिंग, महाराष्ट्र में पैट, उत्तराखंड में गुल, हिमाचल प्रदेश में कुल और और जम्मू में कुहाल कुछ ऐसे पारंपरिक जल-संवर्धन के सलीके थे जो आधुनिकता की आंधी में कहीं गुम हो गए और अब आज जब पाताल का पानी निकालने व नदियों पर बांध बनाने की जुगत अनुतीर्ण होती दिख रही हैं तो फिर उनकी याद आ रही है। गुजरात के कच्छ के रण में पारंपरिक मालधारी लोग खारे पानी के ऊपर तैरती बारिष की बूंदों के मीठे पानी को ‘विरदा’ के प्रयोग से संरक्षित करने की कला जानते थे। सनद रहे कि उस इलाके में बारिश भी बहुत कम होती है। हिम-रेगिस्तान लेह-लद्दाक में सुबह बरफ रहती है और दिन में धूप के कारण कुछ पानी बनता है जो शाम को बहता है। वहां के लोग जानते थे कि शाम को मिल रहे पानी को सुबह कैसे इस्तेमाल किया जाए।
तमिलनाडु में एक जल सरिता या धारा को कई कई तालाबों की श्रंखला में मोड़कर हर बूंद को बड़ी नदी व वहां से समुद्र में बेजा होने से रोकने की अनूठी परंपरा थी। उत्तरी अराकोट व चेंगलपेट जिले में पलार एनीकेट के जरिए इस ‘‘पद्धति तालाब’’ प्रणाली में 317 तालाब जुड़े हैं। पानी के कारण पलायन के लिए बदनाम बंुदेलखंड में भी पहाडी के नीचे तालाब, पहाडी पर हरियाली वाला जंगल और एक तालाब के ‘‘ओने’’(अतिरिक्त जी की निकासी का मुंह) से नाली निकाल कर उसे उसके नीेचे धरातल पर बने दूसरे तालाब से जोड़ने व ऐसे पांच-पांच तालाबों की कतार बनाके की परंपरा 900वीं सदी में चंदेल राजाओं के काल से रही है। वहां तालाबों के आंतरिक जुड़ावों को तोड़ा गया, तालाब के बंधान फोड़े गए, तालाबों पर कालोनी या खेत के लिए कब्जे हुए, पहाड़ी फोड़ी गई, पेड़ उजाड़ दिए गए। इसके कारण जब जल देवता रूठे तो पहले नल, फिर नलकूप के टोटके किए गए। सभी उपाय जब हताश रहे तो आज फिर तालाबों की याद आ रही है।
जल को सोच समझ कर खर्च करना तो जरुरी है है ही, आकाश से गिरी हर बूँद को सहेज्नेके लिए हमारी पारम्परिक जल संरक्ष्ण प्रणालियों को जिलाना भी अनिवार्य है। ये प्रणालियाँ महज पानी नहीं सहेजती, धरती के बढ़ते तापमान को भी नियंत्रित करती हैं। हरियाली, मवेशी के लिए चारा, भोजन के लिए मछली व अन्य जल- फल के रूप में तो इनका आशीष मिलता ही है।
Disclaimer: यह लेख मूल रूप से पंकज चतुर्वेदी के ब्लॉग पर प्रकाशित हुआ है। इस लेख में अभिव्यक्ति विचार लेखक के अनुभव, शोध और चिन्तन पर आधारित हैं। पंकज चतुर्वेदी पर्यावरण-संबंधी विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं।