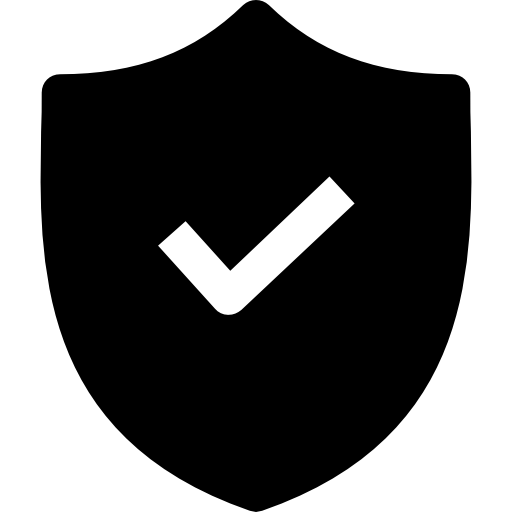जब चवन्नी क्लास में सिनेमा देखने जाने वाली आबादी के लिए सी ग्रेड फिल्में बनती थीं; जब किशोर स्कूलों से भाग कर फिल्में देखते थे; जब बुधवार की रात आठ बजे लोग घरों में और बाज़ार में दुकानों पर रेडियो सीलोन पर अमीन सयानी का बिनाका गीतमाला प्रोग्राम सुनने के लिए वैसे ही जमा होते थे जैसे किसी धार्मिक कथा में; जब लोग चूड़ीबाजे में चाबी भर कर उस पर रिकॉर्ड चलाते और तीन मिनट का गाना सुन कर निसार हो जाते थे; जब पंप से हवा भर कर तथा पिन से उसका नोज़ल साफ कर रसोई में स्टोव जलाते थे, तभी वह वक़्त भी था जब जासूसी कहानियां तथा रोमांस वाले उपन्यास खूब पढे जाते थे। भले ही इनका पढ़ना घरों में त्याज्य था। बड़ों की निगाह बचा कर ही पढ़ना पड़ता था। हालांकि घर के बड़े भी सफर में समय बिताने के लिए ऐसे उपन्यास खरीद कर गटक लेते थे। इसीलिए ऐसे उपन्यास अधिकतर रेलवे स्टेशनों और बसों के अड्डों पर लगी किताबों पर ही सजे मिलते थे। किशोर, पढ़ाई की किताबों में छुपा कर ऐसी कहानियों, उपन्यासों की किताबें और मेग्जीनें पढ़ते थे। उस साहित्य को “लुगदी साहित्य” माना जाता था जो कम दाम पर बेचने के लिए शीघ्र पीले पड़ जाने वाले सस्ते अखबारी कागज पर छापा जाता था। आज की पीढ़ी को यह जान कर हैरानी हो सकती है कि यह साहित्य किताबों की दुकानों तथा विशेष लाइब्रेरियों से प्रतिदिन के हिसाब से किराये पर लाकर भी पढ़ा जाता था। इसी “लुगदी साहित्य” ने पिछली सदी के पांचवें दशक की पीढ़ी में पढ़ने की लत डाली जो उन्हें क्लासिक पढ़ने तक आगे ले जा सकी। उसी पीढ़ी ने घरेलू लाइब्रेरी योजना के सदस्य बन कर हर माह दस पॉकेट बुक्स भी मंगवाई और पढ़ी और उसके जरिए भारतीय और विश्व साहित्य और उनके महान लेखकों से पहला परिचय पाया। इस प्रकार उस पीढ़ी को पढ़ने की जो लत लगी वह ताउम्र उसके साथ रही। कहा भी जाता है कि किशोर वय में जो चीज सीख ली जाती है वह उम्र भर साथ नहीं छोड़ती। लेकिन यह भी सच है कि विद्यार्थियों में पढ़ने की लत हमारी संस्थागत शिक्षा व्यवस्था नहीं डाल सकी और आज हम ऐसे मुकाम पर अपने को पाते हैं जब हर तरफ कहा जा रहा है कि किताबों को अब कौन पढ़ता है? अब तो सभी अपने स्मार्ट फ़ोनों में आंखें गड़ाए रहते हैं। किन्तु दूसरी तरफ हम अपने आसपास तो यही देखते हैं कि धड़ाधड़ किताबें छप रही हैं। इतने नए-नए लेखक और कवि सामने आ रहे हैं, भले ही अनेक रचनाकार अपने खुद के पैसों से अपनी किताबें छपवा रहे हों। लोग धुआंधार लिख रहे हैं और राजकोष से वित्त पोषित अकादमियां उन्हें ढेर सारे इनाम ही नहीं दे रही बल्कि उनको प्रकाशन सहयोग भी दे रहीं हैं। ऐसे में आज के डिजिटल समय में यह पड़ताल जरूरी भी है कि सच में किताबें अब कौन पढ़ रहा है।

किताब उस मुद्रण युग की देन है जो ज्ञान के मौखिक प्रसारण और डिजिटल युग के बीच का काल है। यह काल पश्चिमी जर्मन के शहर मैन्ज़ से शुरू होता है, जहां गुटेनबर्ग ने 1455 में अपना पहला छापाखाना स्थापित किया। गुटेनबर्ग के नवाचार के कारण ही पुस्तकों का छप कर पाठकों के हाथों में पहुंचना संभव हुआ और प्रकाशन व्यवसाय का विकास हो सका। बहुत से अध्येता तो यह भी मानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के जरिए ही संस्कृति, धर्म और ज्ञान में बदलाव आ सके और आगे बढ़ा जा सका। यह भी माना जा रहा है कि डिजिटल के अनुसरण में आगे और भी क्रांतियां होंगी जो मुद्रण की शुरुआत के बाद हुई धार्मिक और सामाजिक उथल-पुथल को प्रतिध्वनित करेंगी। ऐसा मानने वालों को लगता है कि “राष्ट्र” और “राज्य” के विचार को इस नई प्रौद्योगिकी से ही चुनौती मिलेगी। इससे पुराने सामाजिक मानदंड भी बदलेंगे। वे कहते हैं कि पहचान की राजनीति जैसी ऑनलाइन बहसों को जो लोग खारिज करेंगे वे नए ज़माने को समझने का अवसर खो देंगे। इस पड़ताल में एक चीज स्पष्ट नज़र आती है कि छपाई के इतिहास पर तो अनगिनत किताबें लिखी गई हैं, किन्तु पढ़ने के इतिहास पर बहुत कम किताबें हैं। हम कैसे पढ़ते हैं, इस विज्ञान को समझने की ओर ध्यान कम ही गया है। उन्नीसवीं सदी के मध्य में मुद्रण का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, बिल बोर्ड और सस्ते उपन्यास जैसा इतना सामने आया कि दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने समय को “पढ़ने का युग” कहा। लेकिन उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि पाठक के सामने जिस गति और मात्रा में साहित्यिक भोज परोसा जाएगा तो क्या वह कुछ ले भी पाएगा? पश्चिम में वैज्ञानिक प्रयोग करके यह समझने की कोशिश करते रहे हैं कि वास्तव में क्या होता है जब लोग पढ़ते हैं? इन प्रयोगों के मूल में यह विचार रहा कि पढ़ना कोई निष्क्रिय कार्य नहीं है। वह एक सक्रिय काम है। पढ़ने की वैज्ञानिक जांच करने वालों में एक चार्ल्स हब्बार्ड जुड हुए हैं जिन्होंने पढ़ते समय आंखों की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए उपकरण विकसित किया। इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण एडमंड बर्क ह्युई थे, जिनकी कृति ‘द साइकोलॉजी एंड पेडागॉजी ऑफ रीडिंग’ ने 1908 में क्रांति ला दी। जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते होते हैं, की समझ पर उन्होंने पहली बार प्रकाश डाला। ‘टैचिस्टोस्कोप’ का उपयोग करते हुए उन्होंने पाया कि शब्दों को अनुभव से पहचाना जाता है। इस प्रकार, पढ़ना केवल दृष्टि का मामला नहीं है, बल्कि वह याद किए गए, पूर्वानुमानित और अनुमानित अर्थों का मामला भी होता है। उनकी इस अवधारणा ने इस विचार को प्रोत्साहित किया कि पढ़ने को सोचने के रूप में सिखाया जाना चाहिए। इसी प्रकार 1940 के दशक में, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, सैमुअल रेनशॉ ने विमानों की तेजी से पहचान में सुधार करने की कोशिश के अपने युद्धकालीन अनुभव का उपयोग करते हुए हुए ‘स्पीड रीडिंग’ का ज्ञान विकसित किया जिसने 20वीं सदी में, सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने में मदद की क्योंकि तब तक लोकतंत्र के विकास को सुनिश्चित करने में साक्षरता और पढ़ने का महत्व समझा जा चुका था। इस प्रकार स्कूलों में पढ़ना सिखाने का दृष्टिकोण, और सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा निभाई गई भूमिका दुनिया भर में आबादी के बड़े हिस्से को छपी हुई चीजें पढ़ा कर ही लोकतांत्रिक समाज को जोड़ने में महत्वपूर्ण बनी।

एक अध्येता जिसका नई समझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वह है मार्शल मैक्लुहान। उसके ‘द गुटेनबर्ग गैलेक्सी’ (1962) ने मीडिया युग के “नैतिक आतंक” के बारे में लोगों के विचारों को गहराई तक प्रभावित किया। उसका तर्क था कि समाज को यह समझने में देर हो गई है कि “माध्यम ही संदेश है”। मैकलुहान ने यह भी कहा कि मुद्रित पृष्ठ “मन की अनोखी आदतों का निर्माता” होता है। इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अनुभूति की मानसिक प्रक्रियाओं पर स्क्रीन-रीडिंग के प्रभाव में रुचि रखने वाले न्यूरोवैज्ञानिकों ने हाल के दिनों में वर्तमान तकनीकी रीडिंग के प्रभावों के बारे में चिंता जताई है। अमरीका के नेशनल असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस के अनुसार, 2017 और 2019 के बीच 17 अमेरिकी राज्यों में साक्षरता में गिरावट देखी गई जिसके लिए पढ़ने में आए बदलाव को जिम्मेवार माना जा रहा है। किन्तु क्या यूट्यूब और टिकटॉक के युग में पढ़ना अब भी एक जरूरी कौशल के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें सभी नागरिकों को दक्ष हों? अध्येताओं का कहना है कि पढ़ने के कौशल, और जो पढ़ा जाता है उसकी समझ, को सभी के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए कैसे सुलभ बना सकते हैं इस पर काम करना जरूरी है क्योंकि इसका उनके जीवन की संभावनाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। पढ़ने और लिखने दोनों के क्षेत्र में अब चैट जीपीटी प्रवेश कर चुका है जिसके लिए तो यहां तक कहा जाने लगा है कि इससे हमें खुद पाठों (टेक्स्ट) को पढ़ने और समझने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हमारा यह बोझ कंप्यूटर का ‘एल्गोरिद्म’ उठा लेगा। इस प्रकार मशीनी बुद्धि ‘एआई’ द्वारा सक्षम किए गए अत्यधिक “डेटाफिकेशन” के कारण हमें पारंपरिक पढ़ने को बड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। हालांकि अतीत में किताबों का वृहद उत्पादन और पढ़ने का अभ्यास जबरदस्त तरीके से प्रभावशाली रहा है, मगर अब आगे क्या होगा जब एल्गोरिद्म मनुष्यों की तुलना में अधिक रीडिंग करने लगेगा? उससे समाज कैसे बदल जाएगा उसकी चिंता बहुतों को सता रही है। पब्लिशर्स वीकली ने भी हाल ही में बताया कि इस साल की पहली छमाही के लिए किताबों की बिक्री एक बार फिर कम हो गई है। किताबों की बिक्री में गिरावट कोविड महामारी के बाद से ही जारी है। अनेक पाठक अब कागज की बंधी किताब को छोड़ कर जब ‘किंडल’ (डिजिटल किताब) की राह पर भी हो लिए हैं जिसे मशीन बोल कर सुना भी सकती है। फिर भी ऐसे लोग अब तक बचे हुए हैं जो भौतिक रूप में किताबों को पसंद करते हैं। किताबों की गंध, उनका अनुभव, पढ़ने का संवेदी अनुभव उन्हें सुकून देता है। वे सीने पर किताब रखे सो भी जाते है। ऐसे लोग भी हैं जो किताब खरीदना एक नेक काम मानते हैं। ऐसे ही नेक लोग “किताबें कौन पढ़ता है” के झंझावात में नांव को थामे रखने की अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यह भरोसा देता है कि किताबें रहेंगी और हाथ में लेकर उन्हें पढ़ने वाले भी रहेंगे।