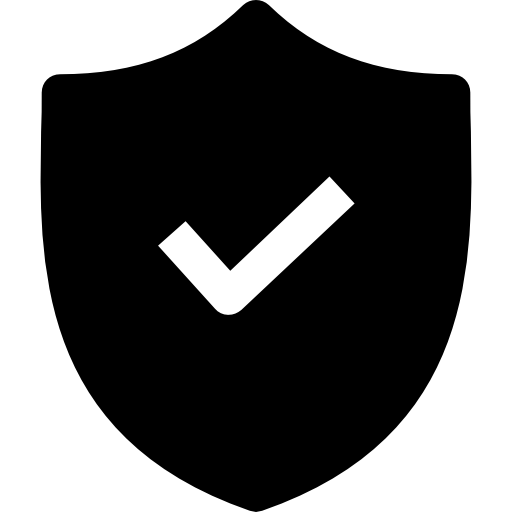एक समय न्यायिक सक्रियता का हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट, जनहित के मुद्दे पर मुखर और आक्रामक थी। आज भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। एक जनहित याचिका अदालत में दायर होती है, जब उस पर अदालत का निर्णय आता है और सरकार, उस पर कार्यवाही करने को बाध्य हो जाती है। जनहित याचिका या पीआईएल ने बहुत से क्षेत्रों, कारागार और बन्दी, सशस्त्र सेना, बालश्रम, बंधुआ मजदूरी, शहरी विकास, पर्यावरण और संसाधन, ग्राहक मामले, शिक्षा, राजनीति और चुनाव, लोकनीति और जवाबदेही, मानवाधिकार और स्वयं न्यायपालिका पर भी असर डाला है। इस परिवर्तन को, ज्यूडिशियल एक्टिविज़्म या न्यायिक सक्रियता शब्द दिया गया, जिसका मध्यम वर्ग ने खूब, स्वागत और समर्थन किया । तब जस्टिस भगवती ने कहा था कि, एक पोस्टकार्ड को भी, अगर वह जनता के व्यापक सरोकारों से जुड़ा है तो, सुप्रीम कोर्ट उसे जनहित याचिका मान कर सुनावायी करेगी।
जनहित याचिका, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जनता के मूल मुद्दों को, एक याचिका के माध्यम से, न्यायालय के समक्ष रखा जाता है, और न्यायालय अपने अधिकार और शक्तियों के अंतर्गत, सरकार या जिसे वह चाहे, उन मुद्दों के समाधान के लिये उचित आदेश, निर्देश देती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि, ऐसी याचिकाएं, जो पीड़ित हो या पीड़ित का कोई परिचित या रिश्तेदार हो, वही दायर करे, बल्कि ऐसी याचिकाएं कोई भी दायर कर सकता है। जनहित याचिका की अवधारणा, न्यायिक सक्रियता के काल की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन यह आवश्यक है कि, ऐसी याचिकाएं, जनहित से ही जुड़ी हों और उनके पीछे कोई अन्य उद्देश्य न हो।
अब यह सवाल उठता है कि, ऐसी याचिकाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी ? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सोचा कि सामान्य जनता के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिये सुप्रीम कोर्ट जा सके और जनहित की बात उठा सके। इसलिए ऐसी याचिकाओं द्वारा जनहित के समाधान की बात सोची गयी कि, कोई भी व्यक्ति या संस्था, व्यापक जनहित के मुद्दे पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपना निवेदन कर सकती है। अदालत ने भी व्यापक जनहित के मुद्दों के समाधान के लिये, स्वतः संज्ञान लेने की परंपरा भी शुरू की।
जनहित याचिका जैसा कोई प्राविधान, संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से व्युत्पन्न है, इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय समतुल्य भी नहीं है। इसे भारतीय न्यायपालिका का एक प्रगतिशील और जनहितकारी कदम कहा जा सकता है। इस प्रकार की याचिकाओँ का विचार पहले पहल, अमेरिका में जन्मा। वहाँ इसे ‘सामाजिक कार्यवाही याचिका’ कहते है। भारत में जनहित याचिका के परंपरा की शुरुआत, जस्टिस पीएन भगवती ने की थी। ऐसी याचिकाएँ लोक के व्यापक हित की भावना पर आधारित होती हैं। इनका लक्ष्य जनहित के लिये एक संवेदनशील प्रशासन का मार्ग प्रशस्त करना, जनता को, सस्ता न्याय दिलवाना तथा कार्यपालिका विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य से विचलित न होने देना है।
जनहित याचिकाओं की स्वीकृति हेतु उच्चतम न्यायालय ने कुछ नियम बनाये हैं, जैसे,
- लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन पीआईएल दायर कर सकता है।
- कोर्ट को दिये गया पोस्टकार्ड को भी रिट याचिका मान कर उस पर कार्ययवाही की जा सकती है
- कोर्ट को अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ कर दे।
- यह राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरूद्ध भी लायी जा सकती है।
जनता को इस प्राविधान से निम्न लाभ भी मिले,
- इस याचिका से जनता में स्वयं के अधिकारों तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे में चेतना बढ़ी और मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता आयी।
- यह कार्यपालिका और विधायिका को, अपनी संवैधानिक मर्यादा में रहने के लिये बाधित करती है।
वर्ष 1976 में, मुम्बई में, श्रमिको की कुछ समस्याओं को लेकर, उनके एक अपंजीकृत संगठन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, एक याचिका दायर करने की अनुमति, जस्टिस कृष्ण अय्यर ने पहली बार दी। जस्टिस अय्यर ने नियमों के शिथिल करने के पीछे, जो कारण बताए, वे ही आगे चल कर, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,के मुकदमे के रूप में जनहित याचिका के अवधारणा की पीठिका बनी। तब यह तय हुआ, कि, कोई भी व्यक्ति जिसका उस समस्या से कोई संबंध न हो, तो, वह भी, अदालत में कोई याचिका दायर करके, किसी अन्य की या किसी सामुहिक समस्या के बारे में न्यायिक राहत पा सकता है।
यहा एक लोकस स्टैंडाई का महत्वपूर्ण कानूनी विंदु उठता है कि कोई असंबद्ध व्यक्ति कैसे किसी अन्य की समस्या के बारे में, याचिका दायर कर सकता है ? पर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में, लोकस स्टैंडाई के प्रश्न को नए सिरे से परिभाषित किया, और कहा कि, किसी जनहित की समस्या के बारे में कोई भी जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता या संगठन किसी व्यापक जनहित की समस्या के बारे में याचिका दायर कर सकते हैं। यह याचिकायें, संविधान के अनुच्छेद, 32 के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में, दायर की जा सकती है।
अब कुछ महत्वपूर्ण उन जनहित याचिकाओं की चर्चा की जाती है जिन्होंने, न्याय अदालत और कानून के दायरे को असीमित तो किया ही है, जनता में भी यह भरोसा पैदा किया कि उसकी बात अब अनसुनी नहीं रहेगी।
राजस्थान का विशाखा का मुकदमा एक प्रसिद्ध मुकदमा है जिसके आधार पर सरकार ने नए नियम और कानून बनाये। कार्यस्थल पर होने वाले यौन-उत्पीड़न के ख़िलाफ़ साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे. सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को ही ‘विशाखा गाइडलाइन्स’ के रूप में जाना जाता है। इसे विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार मामले के तौर पर भी जाना जाता है। इस फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यौन-उत्पीड़न, संविधान में निहित मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15 और 21) का उल्लंघन हैं. इसके साथ ही इसके कुछ मामले स्वतंत्रता के अधिकार (19)(1)(g) के उल्लंघन के तहत भी आते हैं.
राजस्थान में जयपुर के पास भातेरी गांव में रहने वाली सोशल वर्कर भंवरी देवी इस पूरे मामले की केंद्र-बिंदु रहीं। भंवरी देवी राज्य सरकार की महिला विकास कार्यक्रम के तहत काम करती थीं। एक बाल-विवाह को रोकने की कोशिश के दौरान उनकी बड़ी जाति के कुछ लोगों से दुश्मनी हो गई. जिसके बाद बड़ी जाति के लोगों ने उनके साथ गैंगरेप किया. इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो बड़े पदों पर थे। न्याय पाने के लिए भंवरी देवी ने इन लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कराया लेकिन सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया क्योंकि गांव पंचायत से लेकर पुलिस, डॉक्टर सभी ने भंवरी देवी की बात को सिरे से ख़ारिज कर दिया था।
भंवरी देवी के ख़िलाफ हुए इस अन्याय ने बहुत से महिला समूहों और गैर-सरकारी संस्थाओं को आगे आने के लिए विवश कर दिया। कुछ ग़ैर-सरकारी संस्थाओं ने मिलकर साल 1997 में ‘विशाखा’ नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. जिसे विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इस याचिका में भंवरी देवी के लिए न्याय और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन-उत्पीड़न के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई।
उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए यौन उत्पीड़न को नए तरह परिभाषित किया। 1997 से पहले महिलाएं कार्यस्थल पर होने वाले यौन-उत्पीड़न की शिकायत आईपीसी की धारा 354 (महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले ) और 509 (किसी औरत के सम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात या हरकत) के तहत दर्ज करवाती थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन्स के तहत कार्यस्थल के मालिक के लिए ये ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की थी कि, किसी भी महिला को कार्यस्थल पर बंधक जैसा महसूस न हो, उसे कोई धमकाए नहीं. साल 1997 से लेकर 2013 तक दफ़्तरों में विशाखा गाइडलाइन्स के आधार पर ही इन मामलों को देखा जाता रहा लेकिन 2013 में ‘सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्कप्लेस एक्ट’ आया। जिसमें विशाखा गाइडलाइन्स के अनुरूप ही कार्यस्थल में महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात कही गई. इसके साथ ही इसमें समानता, यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्यस्थल बनाने का प्रावधान भी शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत किसी भी महिला को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह की कार्रवाई का सहारा लेने का अधिकार है।
हरियाणा का एक प्रकरण है जिंसमे सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिये, किसी प्रत्याशी के दो बच्चों से अधिक न होने की शर्त को सही ठहराया है। यह मामला है जावेद बनाम हरियाणा राज्य का। पंचायत चुनाव में जावेद नामक प्रत्याशी का निर्वाचन इसलिए रद्द कर दिया गया कि उसे दो बच्चों से अधिक संतान थी, और राज्य के पंचायती राज कानून के अनुसार, दो संतानों से अधिक रखने वाले प्रत्याशी, चुनाव नहीं लड़ सकते है। जावेद ने इस प्राविधान को चुनौती दी और यह मामला, सुप्रीम कोर्ट तक गया। अदालत ने इसकी सुनवाई कर के इस प्राविधान को बहाल रखा और, इसे जनसंख्या नियंत्रण की ओर एक जनहितकारी कदम और उचित प्राविधान माना।
पीआईएल का प्रमुख उदाहरण, 1979 में हुसैनआरा खा़तून और बिहार राज्य का मुकदमा है। इस केस में कारागार और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया था। यह मामला, एक अधिवक्ता द्वारा, दि इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक खबर, जिसमें बिहार के जेलों में बन्द हजारों विचाराधीन कैदियों का हाल वर्णित था, के आधार पर दायर किया गया था। मुकदमे के काऱण, 40,000 से भी ज्यादा कैदियों को रिहा किया गया था। त्वरित न्याय को एक मौलिक अधिकार माना गया, जो उन कैदियों को नहीं दिया जा रहा था। इस सिद्धांत को बाद के मुकदमो में भी स्वीकार किया गया।
एमसी मेहता और भारतीय संघ और अन्य का मुुकदमा, जो 1998 से 2001 तक चला में, अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली मास्टर प्लान के तहत और दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिये दिल्ली के रिहायशी इलाकों से करीब एक लाख औद्योगिक इकाईयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाय। इस फैसले ने वर्ष 1999 के अंत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक अशांति और सामाजिक अस्थिरता को भी जन्म दिया था और इसकी आलोचना भी कुछ लोगों ने की थी कि यह कदम मजदूरों के हित और उनकी रोजी रोटी पर असर डालेगा, पर पर्यावरण और बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के लिये यह ज़रूरी था कि, ऐसे कदम उठाए जांय और उद्योगों के लिये कोई अन्य वैकल्पिक जगह दी जाय। हालांकि इस पीआईएल के काऱण लगभग बीस लाख लोग प्रभावित हुए, जो उन इकाईयों में सेवारत थे।
इसी से जुड़े एक अन्य, फैसले में उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2001 में आदेश दिया कि, दिल्ली की सभी सार्वजनिक बसों को चरणबद्ध तरीके से सिर्फ सीएनजी (कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) ईंधन से चलाया जाए। क्योंकि यह माना गया कि सीएनजी, डीज़ल की अपेक्षा कम प्रदूषणकारी है। हालाँकि बाद में यह भी पाया गया कि बहुत कम गंधक वाला डीज़ल भी एक अच्छा या बेहतर विकल्प हो सकता है।
पर्यावरण, महानगरों की एक बड़ी समस्या है और यह एक वैश्विक समस्या है। दुनियाभर के देश अपनी अपनी तरह से इस समस्या से निपटने के लिये प्रयासरत है। एमसी मेहता की याचिका से, लोग प्रभावित भी हुए और उनकी आलोचना भी की गयी पर जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सरकार ने कार्यवाही की तो उसके सुखद और बेहतर परिणाम भी मिले।
ऐसा नही कि सुप्रीम कोर्ट के इस सदाशयता से भरे प्राविधान का दुरुपयोग नहीं हुआ है। दुनिया मे एक भी कानून ऐसा नहीं बना है, जिसका दुरुपयोग न हुआ हो। मनुष्य की कुटिल मेधा हर कानून में कोई न कोई छिद्र ढूंढ ही लेती है।
जनहित की आड़ में, स्वहित या अन्य स्वार्थ की बाते भी सामने आयी हैं। जब जनहित याचिकाओं पर त्वरित कार्यवाही होने लगी तो बहुत सी ऐसी याचिकाएं भी दायर होने लगीं जिनका सरोकार, प्रचार पाना था और स्वयं उच्चतम न्यायालय ने एक पीआईएल में यह कहा, “अगर इसको सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया और इसके दुरुपयोग को न रोका गया, तो यह अनैतिक हाथों द्वारा प्रचार, प्रतिशोध, निजी या राजनैतिक स्वार्थ का हथियार बन सकता है।”
भारत के मुख्य न्यायधीश के जी बालाकृष्णन ने 8 अक्टूबर 2008 को सिंगापुर लॉ अकादमी में दिये गये अपने भाषण में पीआईएल की अनिवार्यता और महत्व दुहराते हुए यह भी माना कि ” पीआईएल द्वारा न्यायालय मनमाने तरीके से विधायिका के नीतिगत फैसलों में दखल दे सकता है, और ऐसे आदेश दे सकता है जिनका क्रियान्वयन कार्यपालिका के लिये कठिन हो और जिससे सरकार के अंगों के बीच के शक्ति संतुलन की अवहेलना हो। ”
उन्होंने यह भी माना कि ” पीआईएल ने बेमतलब केसों को भी जन्म दिया है जिनका लोक-न्याय से कोई सरोकार नहीं है। न्यायालय में मुकदमों की संख्या बढ़ाकर इसने न्यायालय के मुख्य काम को प्रभावित किया है और माना कि जजों के अपने अधिकारों से आगे बढने की स्थिति में कोई जाँच प्रक्रिया भी नहीं है। ”
जस्टिस भगवती के क्रांतिकारी कदम के बाद न्यायपालिका जनता के राहत के लिये अंतिम आश्रय के रूप में धीरे धीरे प्रतिष्ठित हो गई लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था, तब ऐसा नहीं था। 19 मई 1950 को एके गोपालन बनाम राज्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 की शाब्दिक व्याख्या करते हुए यह फैसला दिया गया था कि, ” अनुच्छेद 21 में व्याख्यित ‘विधिसम्मत प्रक्रिया’ का मतलब सिर्फ उस प्रक्रिया से है जो किसी विधान में लिखित हो और जिसे विधायिका द्वारा पारित किया गया हो।”
अर्थात्, अगर भारतीय संसद ऐसा कानून बनाती है जो किसी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार से अतर्कसंगत तरीके से वंचित करता हो, तो वह मान्य होगा। न्यायालय ने यह भी माना कि अनुच्छेद 21 की विधिसम्मत प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय या तर्कसंगतता शामिल नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना कि अमरीकी संविधान के उलट भारतीय संविधान में न्यायालय विधायिका से हर दृष्टिकोण में सर्वोच्च नहीं है और विधायिका अपने क्षेत्र (कानून बनाने) में सर्वोच्च है।
इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई । यह उच्चतम न्यायालय के आरंभिक वर्ष थे जब इसका रुख सावधानीभरा और विधायिका समर्थक था। यह काल हर तरह से, आज के माहौल, जब न्यायिक समीक्षा की अवधारणा स्थापित हो चुकी है और न्यायालय को ऐसी संस्था के रूप में देखा जाता है जो नागरिकों को राहत प्रदान करता है और नीति-निर्माण भी करता है जिसका राज्य को पालन करना पड़ता है, से भिन्न था। बाद के फैसलों में, न्यायालयों की सर्वोच्चता स्थापित हुई और इस बीच विधायिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद और संघर्ष भी हुआ।
गोलक नाथ और पंजाब राज्य ( 1967 ) केस में 11 जजों की खंडपीठ ने माना कि संसद ऐसा संविधान संशोधन पारित नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। केशवानंद भारती और केरल राज्य ( 1973 ) केस में उच्चतम न्यायालय ने गोलक नाथ निर्णय को रद्द करते हुए यह दूरगामी सिद्धांत दिया कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान की मौलिक संरचना को बदलने वाला संशोधन करे और यह भी माना कि न्यायिक समीक्षा मौलिक संरचना का भाग है। आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर तथा अन्य बनाम शिवकांत शुक्ला ( 1976) केस, में न्यायालय ने कार्यपालिका को नागरिक स्वतंत्रता और जीने के अधिकार को प्रभावित करने की स्वछंदता दी थी, का भी योगदान माना जाता है। इस फैसले ने अदालत के नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक होने की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लगा दिया। आपातकाल ( 1975 – 76 ) के पश्चात् न्यायालय के रुख में गुणात्मक बदलाव आया और इसके बाद पीआईएल के विकास को कुछ हद तक इस आलोचना की प्रतिक्रिया के रूप में देख सकते हैं।
क्या न्यायपालिका, लोककल्याणकारी राज्य और विधि के शासन की उदात्तता को आगे बनाये रख सकेगी, यह आज के माहौल में एक ज्वलंत प्रश्न है। न्यायपालिका के सामने अपनी भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए विधायिका और कार्यपालिका पर उसे निर्भर रहना पड़ता है। न्यायपालिका अपनी लाख स्वतंत्रता के बावजूद, एक राज्य के अंतर्गत राज्य के रूप में विकसित नहीं हो सकती है। लेकिन जनता के अंतिम आश्रय के रूप में वह राज्य के शेष अंगों की तुलना में कहीं अलग और विश्वसनीय ठहरती है। आज भी सुप्रीम कोर्ट की साख है और तमाम आलोचनाओं के बाद भी उम्मीद न्यायपालिका से है।
बदलते समय के अनुसार, जब सरकार के लोककल्याणकारी राज्य का एजेंडा, धीरे धीरे बेहद शातिर और पोशीदा तऱीके से, बदल रहा है तो ऐसे समय मे न्यायपालिका को जनहित के मुद्दों और लोककल्याणकारी राज्य की मौलिक सोच के पक्ष में जम कर खड़ा होना होगा। अब यह भविष्य ही बता पायेगा कि, बदलाव के इस जटिल और कठिन समय मे सुप्रीम कोर्ट कहां होगा और उसकी भूमिका क्या रहेगी। हमें बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए।