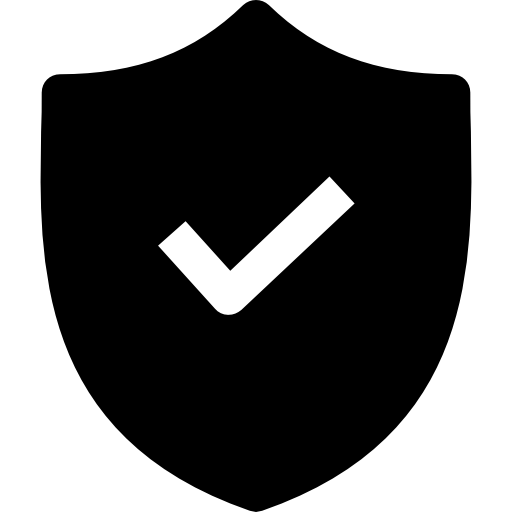लोकतान्त्रिक व्यवस्था में पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए विधायिका का नियमित निर्वाचन शासन में जन भागीदारी का महत्वपूर्ण घटक है। भारतीय संविधान में सार्वभौम सत्ता यहां के नागरिकों के हाथ में हैं जो अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करते हैं। जो जनता का बहुमत जुटा पाता है वही शासन की बागडोर संभालता है। परंतु दलीय लोकतंत्र में मंत्रीमंडल का सामूहिक दायित्व होता है, भले ही उसका गठन विधायिका में बहुमत वाला नेता करता है। प्रत्येक पांच साल बाद राजनेताओं को फिर से जनता के दरबार में जाना होता है और उनके बहुमत का समर्थन पाना होता है। राजस्थान में वह घड़ी आ गई है कि जब यहां के लोग आगामी 23 नवंबर को अपने दो सौ नुमाइंदे चुनने के लिए मतदान करेंगे और तीन दिसंबर को वोटिंग मशीनें परिणाम बता देंगी कि अगले पांच वर्षों के लिए कौन सा दल शासन की बागडोर संभालेगा। शासन में जन भागीदारी की प्रक्रिया अनौपचारिक रूप से दलों के प्रत्याशियों के चयन और निर्दलीय प्रत्याशियों के आगे आने के साथ ही शुरू हो जाती है। मगर जन भागीदारी उतनी आसान नहीं होती जितनी आसानी से उसकी बात की जाती है। विविधताओं वाले भारतीय समाज में सबकी भागीदारी वाली आदर्श गणतांत्रिक व्यवस्था बनाई जाना हमेशा ही कठिन रहा है। सबकी झोली भरे यह भी तो संभव नहीं होता। किन्तु समानता और न्याय की संवैधानिक व्यवस्था का भरोसा सबको एक किये रखता है। दूसरी तरफ यह भी सच है कि शासन में भागीदारी तो सभी चाहते हैं परंतु वास्तविक भागीदारी राजनीति के कुछ धुरंधर चतुर सुजान ही कर पाते हैं। उनकी यह भागीदारी सर्वजनहिताय की न होकर अपने और अपनों के लिये हो कर रह जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक हैं प्रभावी ढंग से भागीदारी के बारे में आम नागरिक के रुझान और उसमें जागरूकता की कमी। हर पांच साल में एक बार ‘हम भारत के लोग’ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों में वोट देकर इन सदनों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और आम तौर पर इसे ही लोकतंत्र में जन भागीदारी मान ली जाती है। वर्ष 2009 में मतदान के 58 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 67 प्रतिशत होने के साथ, यह कहना सुरक्षित भी हो गया है कि आधे से अधिक राष्ट्रीय आबादी इस माध्यम से अपने शासन के साथ जुड़ती है। जन भागीदारी के लिए सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकार से पारदर्शिता, जवाबदेही और जवाब मांगने के अधिकार की गारंटी देता है किन्तु वह भी शासन तंत्र के प्रपंच में अपनी अपेक्षित धार खो देता है। शासन तंत्र अर्थात कार्यपालिका की जवाबदेही बनाए रखने की जिम्मेदारी निर्वाचित प्रतिनिधियों अर्थात विधायिका पर होती है वह जब कर्तव्यच्युत होने लगे तब जन भागीदारी की अहमियत और बढ़ जाती है क्योंकि उसी से गणतंत्र का कारोबार सही तरीके से चल सकता है। संसद के ऊपरी और निचले सदनों व विधानसभाओं की कार्यवाहियों का प्रसारण भी जन भागीदारी को बढ़ावा देने का एक जरिया है। सदन की इन कार्यवाहियों को देख कर नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों और सत्ता में बैठे नेतृत्व के प्रदर्शन की गहरी समझ पा सकते हैं। इससे नागरिकों को मतदाता के रूप में अपने भविष्य के विकल्प चुनने के लिये दृष्टि बनती है। सदनों की वेबसाइटें नागरिकों को कार्यवाही के विवरणों तक आम नागरिकों को पहुंच प्रदान करती है, जिसमें सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रश्न और उनके उत्तर भी शामिल हैं। मगर यह सब तब निरर्थक हो जाता है जब आम नागरिक उदासीन हो। आम जन की उदासीनता एक ऐसे राजतन्त्र को मजबूत करता है जो गणतांत्रिक व्यवस्था में गण के साथ सहकार नहीं करता। राजा और प्रजा जैसा सामंती नाता ही बना रहता है।
लोकतांत्रिक सिद्धांत उन लोगों के माध्यम से लागू किये जाते हैं जिनके पास निर्णय लेने का अधिकार होता है। “हम भारत के लोग” निर्णय लेने का अपना अधिकार विधायकों और सांसदों को अपना प्रतिनिधि बना कर हस्तांतरित कर देते हैं। व्यवहार में नागरिक अपने जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियां और कार्यक्रम खुद नहीं बनाते। उनका मतदान सिर्फ अपने प्रतिनिधि चुनने तक सीमित होता है। नागरिकों के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाली नीतियां और कार्यक्रम बनाने का काम उनके लिए सरकार चलाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों पर छोड़ दिया जाता है जो उसे आगे नौकरशाहों को सौंप देते हैं। सत्ता में बैठे लोग जनता से उनका विज़न मांगने का ढोंग जरूर करते रहते हैं। यही कारण है कि देश के संसाधनों और संपत्ति का लोकतांत्रिक तरीके से वितरण नहीं हो पाता हैं। हाल ही में यह आंकड़ा सामने आया है कि देश की 77 प्रतिशत से अधिक संपत्ति 10 प्रतिशत आबादी के हाथ में है। राजनैतिक व्यवस्था में सभी स्तरों पर पहले से राज में भागीदारी पा रहे नेताओं के ऐसे निहित स्वार्थ बन जाते हैं कि वे अन्यों को अपने प्रभुत्व के लिए खतरा मानने लगते हैं और केवल उन्हीं लोगों के साथ सहज होते हैं जो उनकी छत्र-छाया में रहने को राजी होते हैं। इस व्यवस्था में वंश, परिवार, जाति, क्षेत्र और धर्म के हितों का जाल ऐसा फैला दिया जाता है कि समग्र जनहित की बात औपचारिकता मात्र बन कर रह जाती है। राजनीति में जनशिक्षण अतीत की बात हो गई है। राजनेता और राजनीतिक कार्यकर्ता सत्ता में आने और वहां रहने के लिए समर्पित रहने लगे हैं क्योंकि राजनीति अब एक कारोबार बन गई है। युवा वर्ग अपने-अपने जाति समूहों के बल पर छात्र जीवन से ही राजनीति को पेशे के तौर पर अपनाने के जतन करने लगता है ताकि सत्ता के बाजार में वह अपना मोल बढ़ा सके। ऐसे में यह सवाल भी है कि राजनेताओं तथा राजनीतिक संस्थानों में नागरिकों का भरोसा कैसे बना रह सकता है?
राजनीतिक भरोसे में बदलाव का होना लोकतंत्र के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण में बदलाव तथा आर्थिक माहौल में बदलाव से भी जुड़ा होता है। इसी कारण वैचारिक ध्रुवीकरण में बदलाव और लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था से नागरिकों की संतुष्टि के बीच भी संबंध देखा जा सकता है। राजनेता जनभागीदारी की बात अपनी सत्ता के लिए करते हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों अचानक लोकलुभावन घोषणाओं तथा राहतों तथा उनके प्रचार का जबरदस्त विस्फोट नज़र आया। लोकलुभावन चीजें लोकतंत्र विरोधी नहीं होती, मगर वे किस कीमत पर होती हैं और उनका क्या दीर्घकालीन प्रभाव होने वाला है उसकी जानकारी मतदाता को नहीं होती क्योंकि वह अपनी भागीदारी के बारे में गंभीर नहीं होता। राष्ट्रवाद भी लोक लुभावन लहर ही होता है। अब सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों के माध्यम से राजनीतिक विचारधाराएं अपना वर्चस्व खोजने लगी हैं। शासन भी इन्हीं प्लेटफार्मों पर जन भागीदारी का आसान रास्ता अपनाने लगा है। ऐसा मानने वाले भीकम नहीं हैं कि सोशल मीडिया, नागरिक भागीदारी की ताकत और अवसर देता है। वह नागरिकों को विभिन्न मुद्दों पर अपने विचारों को व्यक्त करने का विकल्प देता है। किन्तु सोशल मीडिया का माध्यम आदर्श मानवीय एकता को खंडित भी करता है। आभासी दुनिया पर व्यक्तियों के समूह बनते हैं जिनमें अपनी बात को मनवाने की आपसी प्रतिस्पर्धा होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपनी बात कहने की होती है, अगले को उसे मानने के लिए बाध्य करने की नहीं होती। सोशल मीडिया पर अलग-अलग समूहों द्वारा अपनी-अपनी अभिव्यक्तियों को धार देते हुए शिष्टाचार की सीमाएं पार कर जाना आम बात है। इससे आपस में तनाव बढ़ता है; भावनाएं भड़कती है। आभासी समूहों का आपसी तनाव बाहर भौतिक दुनिया में उपस्थित हो जाता है। सोशल मीडिया पर वे किरदार अधिक सफल होते हैं जो अपने में कट्टरता भरे रहते हैं। यह कट्टरता किसी एक पक्ष की बपौती जैसी नहीं है। प्रत्येक पक्ष कट्टरता में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता हुआ नज़र आता है। बाज़ार की ताकतें इसमें ऐसी घुल-मिल गई हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन इस प्रतिस्पर्धा को उकसा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म चलाने वालों के पास अपना खुद का कोई माल नहीं होता। वे अपना उपयोग करने वालों के माल से ही अरबों-खरबों कमाते हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों को लगता है वे अभिव्यक्ति की आज़ादी पा रहे हैं और वे जो कुछ कर रहे हैं वह उनका अपना चयन है। मगर आभासी दुनिया के इस भ्रम में लोगों को समूहों में बांट कर कौन अपना खेल कर जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। नये डिजिटल युग में अब तो सोशल मीडिया प्रचार का बड़ा माध्यम बन कर अरबों रुपयों का कारोबार बन गया है। मीडिया के प्रचार के दम पर अब चुनावी मुद्दे बनाये जाते हैं और मतदाताओं को बांटा जाता है। स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के बारे में नागरिक जागरूकता डिजिटल मीडिया तक सीमित होकर रह जाती है। संविधान के दो मौलिक अधिकारों द्वारा समर्थित है- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार। डिजिटल मीडिया ने इन अधिकारों पर कब्जा कर लिया है और लोगों में भेद करने की उसकी उग्रता भौतिक जगत में उतर आने लगी है। दुर्भाग्य से सभी राजनीतिक दलों ने डिजिटल जगत के सोशल मीडिया से जुडने को ही जन भागीदारी की इति मान ली गई है। चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार का मतदाता के साथ सीधा और जीवंत संबंध भी इसी कारण घटता जा रहा है। ऐसे में जनभागीदारी सिर्फ मतदान करने तक रह जाती है।