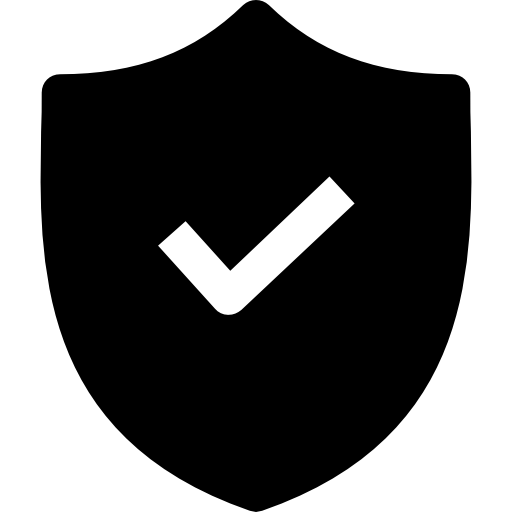डॉ परिवेश मिश्रा : सन 1897 में अपने पिता बिहारीलाल की उंगली पकड़े पांच वर्षीय बालक पालूराम ने हरियाणा के धनाना गांव से निकल कर रायगढ़ में पैर रखे। पास के गांव लोहारी से उनकी बुआ के बेटे किरोड़ीमल कलकत्ता पहुंच गये। इसके लगभग तीस वर्षों के बाद इन मामा-बुआ के बेटों ने मिलकर रायगढ़ के पहले उद्योग की नींव रखी। तब तक सेठ पालूराम धनानिया रायगढ़ में अपने पिता के शुरू किये धान के कारोबार में जम चुके थे। उधर सेठ किरोड़ीमल कलकत्ता में अनुभव, नाम और पैसा कमा चुके थे।
(कलकत्ता के होने के बाद भी सेठ किरोड़ीमल के दान और नाम के निशान देश के कई स्थानों पर मिलते हैं। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक निर्मला काॅलेज था। इसे अमेरिकन जेसुइस्ट नामक संस्था ने शुरू किया था लेकिन 1951 आते तक यह बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। सेठ किरोड़ीमल स्वयं तो अपने नाम के अलावा कुछ लिखना नहीं जानते थे पर शिक्षा का महत्व समझते थे। उन्होने इस बंद होते काॅलेज को खरीद लिया और तीन साल के बाद नाॅर्थ कैम्पस में शिफ्ट कर दिया। अब यह किरोड़ीमल काॅलेज के नाम से जाना जाता है। अमिताभ बच्चन, गिरिजा प्रसाद कोईराला (नेपाल के पूर्व प्रधान म॔त्री) मदनलाल खुराना (दिल्ली के पूर्व मुख्य मंत्री), कुलभूषण खरबंदा जैसे अनेक लोग यहां पढ़े और पढ़ रहे हैं।)
देश में उनके धर्मार्थ कामों का सबसे बड़ा लाभार्थी स्थान रहा रायगढ़। यहां उन्होने एक व्यावसायिक काम भी किया जो था सन् 1928 में जूटमिल की स्थापना। तेईस वर्षीय राजा चक्रधर सिंह ने अपने राज्य में लगभग चालीस एकड़ भूमि इस मिल के लिए उपलब्ध करायी थी।
सारंगढ़, रायगढ़ और उदयपुर (धर्मजयगढ़) राज्यों के इलाकों में पटसन की पैदावार काफी था। हालांकि इतनी भी नहीं थी कि मिल की सतत् आवश्यकता पूरी कर सके। किन्तु एक फ़ैक्टर और था। पूरे मध्य तथा उत्तर-मध्य भारत में उन दिनों कोई जूट मिल नहीं थी। जबकि बारदाने की आवश्यकता सबको थी। इसलिए यदि कुछ अतिरिक्त पटसन बंगाल (तब बांग्लादेश का हिस्सा भी भारत में था) से आयात किया जाता तो भी सौदा मुनाफ़े का ही बैठता था। सोच में कोई खामी नहीं थी।
किन्तु मिल चल नहीं पायी। कहते हैं इतिहास से सबक न लेने पर इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास बना था असम में और दोहराया गया रायगढ़ में।
सन 1820 के दशक में ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारी राॅबर्ट ब्रूस ने असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में स्वाभाविक रूप से उपजे हुए चाय के पौधे देखे। यह तब की बात है जब चीन से अफ़ीम के बदले चाय लेकर इंग्लैंड और योरोप भेजते हुए कई दशक बीत चुके थे। उधर ब्रिटेनवासियों को चाय की लत लग गयी और इधर चीन ने अंग्रेज़ों से अफ़ीम के स्थान पर नगद की मांग रख दी। चाय अंग्रेज़ों के लिए अचानक बहुत महंगी हो गयी। राॅबर्ट ब्रूस की खोज की खबर से उत्साहित ईस्ट इंडिया कम्पनी ने चाय के व्यावसायिक उत्पादन का फ़ैसला कर लिया। चाय बागान शुरू कर दिया गया।
लेकिन प्रयोग असफल हो गया। श्रमिक आधारित इस प्रोजेक्ट की योजना बनाते समय कम्पनी मान कर चली थी कि स्थानीय श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जायेगा। और चूंकि स्थानीय होगा सो अपने रहने खाने की व्यवस्था भी स्वयं कर ही लेगा। हकीकत कुछ और साबित हुई। असमिया ग्रामीण सदियों से चली आ रही अपनी जीवनशैली में रातों रात परिवर्तित लाने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं था। दूसरों के नियंत्रण में उन्होने कभी काम नहीं किया था। कुछ लोगों ने काम शुरू भी किया तो हर दूसरे दिन उन्हें घर और खेत की याद सताती। चार दिन की छुट्टी लेकर जाते तो चौदह दिन में लौटते। अनेक लौटते ही नहीं।
अंत में आजिज़ आकर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने हाथ उठा दिये। इसके बाद दो बातें हुईं। 1839 में चाय उत्पादन का काम नये मालिक “असम कम्पनी” के हाथों में सौंपा गया। पिछले मालिक के अनुभवों से सबक लेकर जो काम असम कम्पनी ने सबसे पहले किया वह था श्रमिकों को बाहर से लाकर बसाने का। श्रमिक सप्लाय करने के लिये ठेकेदारों को नियुक्त किया गया। यहीं से शुरुआत होती है छत्तीसगढ़, झारखण्ड, छोटा नागपुर, और आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों से ले जाये गये श्रमिकों की कहानी। कालांतर में ये “टी-ट्राईब” के नाम से जाने गये।
“टी-ट्राईब” के पहुंचने के बाद नित नये फैलते बागानों को स्थायी मज़दूर मिले। अपनी जड़ों से उखड़कर गये लोग पूर्णकालिक श्रमिक बने और बागान मालिकों के लिए ज़रूरी हो गया कि इनके रहने खाने आदि की व्यवस्था करें। और चाय बागान का कारोबार चल निकला।
अब वापस चलें रायगढ़ की जूट मिल पर। सेठ-द्वय किरोड़ीमल जी और पालूराम जी ने नयी और महंगी मशीनें लगवा कर मिल खड़ी की, बाज़ार ढूंढ़ा और बढ़ाया, लेकिन श्रमिकों की उपलब्धता की जिस आश्वस्ति पर यह सब किया था वह गलत साबित हुई। किसी औद्योगिक इकाई में कार्य करने का पूर्वानुभव न होने के चलते स्थानीय श्रमिकों में कार्य-अनुशासन नहीं था। स्थानीय किसानों को पटसन की पैदावार बढ़ाने की ओर प्रेरित करने के प्रयास भी सफल नहीं हुए। लागत बढ़ना और मुनाफे पर चोट पड़ना स्वाभाविक था। हो सकता है और भी कारण रहे हों।
1935 में रायगढ़ की जूट मिल बिक गयी। खरीदने वाले थे कलकत्ता के सेठ सूरजमल जालान और सेठ नागरमल बजौरिया। आगे चलकर रायगढ़ जूट मिल एक बार और बिकी। इस बार भी खरीददार मारवाड़ी ही थे (श्री पवन कुमार अग्रवाल) और वे भी कलकत्ते के ही रहने वाले थे।
कलकत्ता और मारवाड़ियों का जूट और जूट मिलों से पुराना संबंध रहा है। पूर्वी भारत पारम्परिक रूप से पटसन पैदा करता रहा है। लेकिन भारत में इस पटसन से जूट बनाने की कोई मिल नहीं थी। सारा जूट ब्रिटेन से आयात होता था। ब्रिटेन की सारी जूट मिलों का कच्चा माल रूस से आता था। 1850 के आसपास एक युद्ध हुआ (क्रायमियन वाॅर) जिसमें एक ओर रूस था और दूसरी ओर ब्रिटेन समेत दूसरे देश। स्वाभाविक था इस परिस्थिति में पटसन और अलसी के बीज का ब्रिटेन पहुंचना बंद हो गया।
अब भारतीय पटसन की पूछ बढ़ी। कलकत्ते के पास एक गांव था/है रिशरा। मुगलों के ज़माने में यहां के हिन्दू बुनकरों के हाथों बना सूती कपड़ा और मुस्लिम बुनकरों का बुना रेशम मशहूर था। इसी स्थान पर वाॅरेन हेस्टिंग्स ने बहुत बड़े बगीचे के साथ अपना निजी महल-नुमा घर बनाया था जो उनके जाने के बाद से वीरान पड़ा था। सन् 1855 मे इसी जगह पर भारत की पहली जूट मिल शुरू हुई। इसे एक अंग्रेज़ ने स्थापित किया था।
उस समय तक मारवाड़ी कलकत्ता पहुंच चुके थे। 1860 से पहले उनमें से अनेक ने अफ़ीम, जूट, कपास, अनाज और चांदी के सट्टा बाज़ार में अपार मुनाफ़ा कमाया था। जूट और अफ़ीम के सट्टा बाज़ार पर तो इनका एकाधिकार था। राजस्थान के शेखावाटी इलाके में बारिश होने की संभावना पर सट्टा लगाने की पुश्तैनी आदत साथ ले कर ये लोग बंगाल पहुंचे थे। फतेहपुर के रामदयाल नेवटिया और गजराज सिंघानिया, रामगढ़ के जोखीराम रुईया और नाथूराम पोद्दार, बीकानेर के पनयचंद सिंघी के साथ साथ रतनगढ़ (चुरू) के सूरजमल नागरमल ने भी इस दौरान बहुत धन कमाया था। रामप्रताप चामड़िया ने तो उस ज़माने में करोड़ों रुपये अफ़ीम के सट्टा में कमाये थे। अनेक फ़र्म और व्यक्ति अपना सब कुछ लुटा कर बर्बाद भी हो चुके थे। सट्टे को ये आपसी बातचीत में फटका कहते थे। मारवाड़ियों में एक उक्ति प्रसिद्ध थी :
कर दे बेटा फटको, घर को रहेगो ना घाट को
कर दे बेटा फटको पीयो दूध खायो भात को
सट्टा खेलो। या तो आसमान पर पहुंचोगे या बिल्कुल नीचे ज़मीन पर, बर्बादी पर।
रायगढ़ जूट मिल के नये मालिक भी दानशीलता में अपना नाम दर्ज़ करा चुके थे। रतनगढ़ में रेल्वे स्टेशन, सड़कें, अस्पताल, काॅलेज जैसी अनेक संस्थाओं के साथ इनका नाम दानदाताओं के रुप में जुड़ा रहा है।
सेठ किरोड़ीमल और सेठ सूरजमल नागरमल के कलकत्ता पहुंचने के काल में यह शहर भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करता था। कारोबार में अधिकतर मालिक अंग्रेज़ थे पर काम संभालने वाले मारवाड़ी थे और ये कम्पनी में “बनिया” के औपचारिक पदनाम से जाने जाते थे। जैसे, ओंकार मल जटिया ‘ऐन्ड्रयू-यूल’ के बनिया थे, ताराचंद घनश्याम दास ‘शाॅ-वाॅलेस’ के, रामनारायण रुईया ‘ससून जे. डेविड’ के बनिया थे। इनमें से कई इन कम्पनियों के कमीशन एजेन्ट बने। इन सब से प्राप्त मोटे मुनाफ़े से मारवाड़ियों के पास अच्छी खासी पूंजी इकट्ठा होने लगी थी।
बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में मिलों, कम्पनियों और फ़र्मों के मालिकों के बीच खरीद बिक्री की उथल पुथल रही थी। इसका एक कारण था 1913 से प्रभाव में आया कम्पनी एक्ट। हालांकि तब तक ज़्यादातर फ़र्म ट्रेडिंग का काम ही करती थीं। मैनुफैक्चरिंग में कम लोग थे। इन दशकों में मारवाड़ियों ने अंग्रेज़ों के अधिपत्य में रहा बहुत सा कारोबार खरीदा और बढ़ाया। इनमें ट्रेडिंग फ़र्मों के साथ साथ अनेक जूट मिल, कोयला खदान, तेल मिल आदि भी शामिल थीं।
इस दौर में मारवाड़ियों के हाथों नयी जूट मिलों की स्थापना भी खूब हुई। सेठ किरोड़ीमल का 1928 का उपक्रम भी इनमें शामिल था।
1938 में सेठ सूरजमल की मृत्यु हो गयी (सेठ नागरमल की पहले हो गयी थी)। उन्ही दिनों दूसरा विश्वयुद्ध भी शुरू हो गया और रायगढ़ में काम ढंग से शुरू करना आगे टलता रहा। नयी व्यवस्था में सूरजमल के बड़े बेटे मोहनलाल जालान ने अपने भाईयों बंशीधर, बैजनाथ तथा सेठ नागरमल के बेटों के साथ काम संभाला था। रायगढ़ जूट मिल बाद में मोहन जूट मिल के नाम से जानी गयी।
उन्होने स्थानीय प्रबंधन के लिए सेठ मांगीलाल भंडारी को एजेन्ट और श्री सरावगी को मैनेजर नियुक्त किया। श्रमिक उपलब्धता का समाधान उनके पास पहले से था। कलकत्ता की इनकी मिलों में गोरखपुर के श्री रामसुभग सिंह इस काम के प्रभारी थे और “बड़े- सरदार” कहलाते थे। उनके साथ कलकत्ता में काम कर रहे गोरखपुर और आज़मगढ़ के अलावा बिहार के छपरा के मजदूर रायगढ़ लाये गये (और फिर वे यहीं रच-बस गये)।
आज़ादी के शुरुआती सालों में कांग्रेसी सरकार को मध्यप्रदेश की इस इकलौती जूट मिल के महत्व का अहसास था। श्रम मंत्री रहे श्री गंगाराम तिवारी और श्री वी.वी. द्रविड़, दोनों को इंदौर की मिलों में श्रमिक नेता के रूप में काम करने का अनुभव था और स्थानीय मंत्री राजा नरेशचन्द्र सिंह के साथ इनका अच्छा तालमेल था। इन सब की निगरानी मे मजदूरों के लिए घर बने, सब घरों को बिजली, पानी, शौचालय की सुविधा मिली। खाना पकाने के लिए केरोसिन जैसी चीज़ें मुफ़्त दी गयीं। अन्य हितों की व्यवस्था हुई।
1950 के दशक में मिल में काम करने की इच्छा से आये हुए अनुभवी मजदूर थे। देश और प्रदेश में संवेदनशील और प्रगतिशील सरकारें थीं जो औद्योगिकीकरण भी चाहती थी और मजदूरों का हित संरक्षण भी। मजदूर और मिल मालिक के बीच बैलेंस बनाने में सक्षम मंत्री और विधायक सरकार में थे। रायगढ़ के एकमात्र उद्योग की गाड़ी चल निकली।
(यही मिल आगे चलकर रायगढ़ में नये उद्योगों की स्थापना में कैसे रोड़ा बन गयी, अगले हिस्से में)